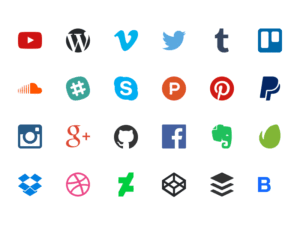
सोशल-मीडिया क्या है? इतिहास, प्रकार, लाभ-हानि और प्रमुख सोशल नेटवर्किंग साइट01
सोशल-मीडिया क्या है? मीडिया :- संचार का माध्यम सामाजिक संजाल स्थल :-सोशल-मीडिया एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को अपने
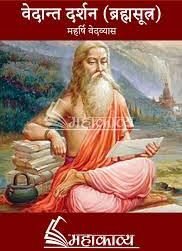
1) बादरायण : समयान्तर में औपनिषद्-सिद्धान्तों में आपाततः विरोध प्रतीत होने के कारण उसका परिहार तथा एक वाक्यता करने के उद्देश्य से महर्षि बादरायण ने ‘ब्रह्मसूत्र’ की रचना की। इसमें ब्रह्मविषयक विवेचन किया गया है।
2) गौडपाद : अद्वैत वेदान्त के प्रथम आचार्य के रूप में आचार्य गौडपाद को माना जाता है। इन्होंने माण्डूक्योपनिषद् पर एक कारिका ग्रन्थ की रचना की जिसका नाम ‘माण्डूक्यकारिका’ है।
3) आचार्य शंकर : अद्वैत वेदान्त के प्रतिष्ठापक आचार्य शंकर ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है जो ‘शारीरकभाष्य’ नाम से विश्वविख्यात है। उनका कर्तृत्त्व अत्यन्त व्यापक है दशोपनिषद्भाष्य, भगवद्गीताभाष्य, उपदेशसाहस्री, विवेकचूडामणि, दक्षिणामूर्तिस्त्रोत, सौन्दर्यलहरी इत्यादि उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं।
4) पद्मपाद – शंकराचार्य के शिष्य पद्मपाद ने शारीरकभाष्य के चतुःसूत्रीपर्यन्त भाग पर ‘पञ्चपादिका’ नामक व्याख्या का प्रणयन किया है। यह ग्रन्थ अद्वैतवेदान्त में ‘विवरणप्रस्थान’ का प्रतिपादक माना जाता है।
5) श्रीहर्ष : श्रीहर्ष ने वेदान्त शास्त्रार्थ पर नव्यन्याय शैली में एक विद्वतापूर्ण ग्रन्थ ‘खण्डनखण्डखाद्य’ का प्रणयन किया है।
6) विद्यारण्य : इन्होंने वेदान्त पर ‘पञ्चदशी’ नामक एक उत्कृष्ट ग्रन्थ की रचना की, जो पद्यबद्ध रूप में है। ‘विवरणप्रमेयसंग्रह’, ‘जीवनमुक्तिविवेक’, ‘वैयासिकन्यायमाला’, ‘दृग्दृश्यविवेक’ आदि भी उनके अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं।
क) ब्रह्म : शंकराचार्य के दर्शन में एकमात्र ब्रह्म ही परम सत्ता है जो अनादि, अनन्त, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान अद्वैत एवं देश-काल से परे है। यही मूल तत्त्व है। यह समस्त जगत् का आधार है। साथ जी यह सर्वोच्च ज्ञान भी है, इसके ज्ञान से ही हमारा अज्ञान नष्ट होता है। यह सच्चिदानन्द स्वरूप है।
‘ब्रह्म’ शब्द ‘बृह’ धातु से बना है, जिसका अर्थ है- ‘बढना’ या ‘विस्तार को प्राप्त होना’ । परमतत्त्व को इसलिए ‘ब्रह्म’ कहा गया है क्योंकि यह सर्वाधिक विस्तृत अर्थात् सबसे महान् सत्ता है, ‘बृहत्तमत्त्वाद् ब्रह्म । ब्रह्म को ही अद्वैत कहा गया है, अद्वैत का अर्थ है- एक ही तत्त्व, जिसे परम सत्ता कहते हैं। उपनिषदों में अद्वैत के विषय में कहा गया है ‘न तु तद् द्वितीयम् अस्ति, ‘नेह नानास्ति किञ्चन आदि।
ख) जगत् : समस्त नामरूप, क्रिया-कारक और उनके फल, जगत् के अन्तर्गत आते हैं (जगतो नामरूपक्रियाकारकफलजातस्य)। आचार्य शंकर ने यद्यपि जगत् के विषय में कई स्थानों पर उसे मिथ्या, मायिक, रस्सी में सर्प के समान भ्रामक कहा है, किन्तु उसे ‘आकाश-कुसुम’ के समान असत् नहीं कहा है।
ग) त्रिविध सत्ता : आचार्य शंकर के अनुसार वे केवल एक ही सत्ता स्वीकार करते हैं इसे वे अद्वैत ब्रह्म कहते हैं, परन्तु अनुभूत पदार्थों के अस्तित्व के लिए वे सत्ता के अन्य स्तर बताते हैं-
घ) माया : आचार्य शंकर के दर्शन में ब्रह्म की रहस्यमयी शक्ति का नाम माया है, जिसके द्वारा ईश्वर जगत् का निर्माण करता है। माया का अर्थ है जो जीव को मोहित करे अथवा जो जीव को मोहित कराये।
माया की दो शक्तियाँ हैं – आवरण शक्ति एवं विक्षेप शक्ति। जो सत्य को ढंकता है अथवा छिपाता है उसे ‘आवरण शक्ति’ कहा गया है, इसी शक्ति के द्वारा माया ब्रह्म के स्वरूप को छिपा देती है, उस पर पर्दा डाल देती है। विक्षेप शक्ति का अर्थ है वास्तविक वस्तु के स्थान पर अवास्तविक को प्रस्तुत करना, जैसे रस्सी सर्प में रस्सी के स्थान पर सर्प की प्रतीति कराना।
च) मोक्ष : अद्वैतवेदान्त के अनुसार जीव एवं ब्रह्म अभिन्न हैं किन्तु जब जीव अपने को ब्रह्म से भिन्न समझता है तो उसका यह अज्ञान ही बन्धन का मूलकारण है। आचार्य शंकर मोक्ष की परिभाषा करते हैं ‘स्वात्मन्यवस्थानम् मोक्षः’ (केनोपनिषद् शांकरभाष्य) अर्थात् आत्मा की अपने स्वरूप में अवस्थिति ही मोक्ष है। अद्वैतमत में मोक्ष नित्य आनन्द की प्राप्ति है।
अद्वैतवेदान्त में मुक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं – जीवनमुक्ति और विदेहमुक्ति। इनके अनुसार मोक्ष, आत्मा का परमात्मा से अभेद ज्ञान है और यह ज्ञान मनुष्य जब जीवितावस्था में ही प्राप्त कर लेता है, यही जीवनमुक्ति है। जीवनमुक्ति के प्रारब्ध कर्मों का जब क्षय हो जाता है तथा शरीर शान्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यही विदेह मुक्ति है।
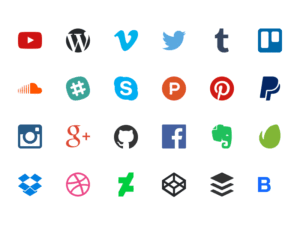
सोशल-मीडिया क्या है? मीडिया :- संचार का माध्यम सामाजिक संजाल स्थल :-सोशल-मीडिया एक ऑनलाइन मंच है जो उपयोगकर्ता को अपने
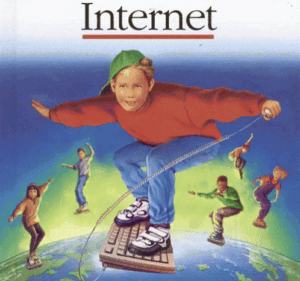
इंटरनेट का परिचय परिचय क्या है– यह दुनिया भर में फैले हुए अनेक छोटे-बड़े कम्प्यूटर नेटवकों के विभिन्न संचार माध्यमों

साइबर अपराध क्या कम्प्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया गैर-कानूनी कार्य या अपराध है । इसे नेट क्राइम

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? क्या है – कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार
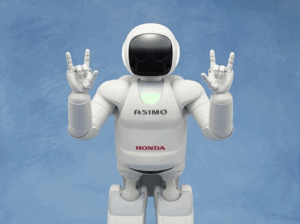
रोबोटिक्स क्या है? क्या है ? – एक मशीन है, जो प्रोग्राम किये गये डाटा के अनुरूप कार्य सम्पादित करती

टेलीविजन का विकासक्रम CRT(cathode-ray tube) आविष्कार कब – 1897 ई। में, कार्ल फर्डिनाण्ड ब्रॉन ने । उपनाम – ब्रौन ट्यूब